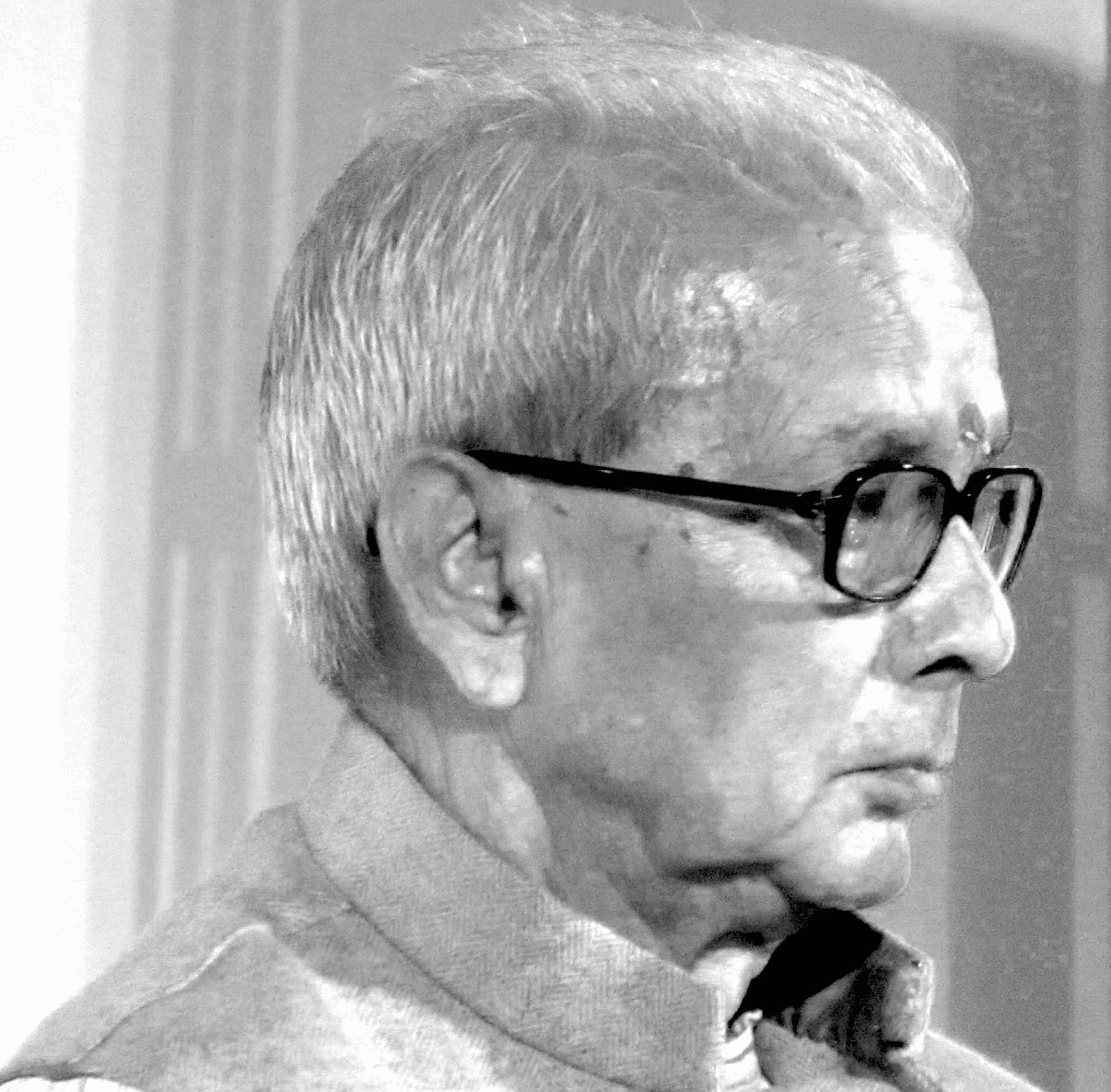कोई अच्छा-सा लेकिन एलिअन भेज दे
विष्णु खरे
मानव शुरू से ही अपने अस्तित्व की समस्याओं से इतना आक्रान्त रहा है कि उसे हर जगह और हर शय में अपने ईश्वर, बुत, फ़रिश्ते, उद्धारक, अवतार स्त्री-पुरुष और नबी-मसीहा खोजने पड़े हैं. विडंबना यह है कि समस्याएँ उतनी ही बढ़ती गई हैं जितने भगवान और पैग़म्बर आए हैं. बल्कि शायद यदि वे कम आए होते, या आते ही नहीं, तो इंसानियत की ऐसी दुर्दशा न होती. अभी जो डेढ़ सौ बच्चे मारे गए हैं उनके पीछे मजहबी थे. मेरठ-गुजरात में भी चोटी-जनेऊ-तिलक-कलावे वाले धर्मप्राण लोग ही बसते हैं. नाइजीरिया में इस्लामी ‘बोको हराम’ ने मानवता का जीना हराम कर रखा है.
जबसे ब्रह्माण्ड के आयामों का पता चला है तबसे यह उम्मीद भी बाँधी गई है कि शायद कहीं ऐसी नस्लें हों जो हम जैसी हों, हम से हजारों गुना विकसित हों, जो हमसे रूबरू या इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से संपर्क साधें और हमारे वुजूद की हिफ़ाज़त करें. हाय रे शिकस्ता ज़ेहनी गुलामी की मजबूरियाँ! लेकिन उसमें यह ख़तरा भी है कि कोई तालिबान, आइ.एस. या हिंदुत्वी-नुमा घुमंतू कायनाती आतंकवादी दस्यु बेड़ा भी हो, जो टेक्नोलॉजी में हमसे सदियों आगे हो लेकिन हर तरह के दूसरे प्राणियों को वाक़ई खाकर ही जिंदा रहता हो, तब हम क्या करेंगे?
जब ‘गाँधीगीरी’ फिल्मों में सुपरहिट रही और भारतीय यथार्थ में सुपरफ्लॉप, तो अब बारी आई है दूसरे ‘गोले’ से आए ‘नेकेड फ़कीर’ ‘पीके’ की. यह भी इसलिए आ सकी कि हमारी दोग़ली इंडस्ट्री के असली गोरे हॉलीवुडी अब्बामियाँ बरसों से विज्ञान-कथा (साइंस-फ़िक्शन) और अच्छे-बुरे एलिअनों का मुफ़ीद इस्तेमाल कर रहे हैं. यह बात अलग है कि अपने भोलेपन में पहली ग़लती सत्यजित राय ने की और हमने अपना ‘महाभारत’ सही ढंग से अब तक नहीं पढ़ा. वैसे हिन्दू मिथकों में सारे भगवान, देवी-देवता, अवतार, ऋषि-मुनि आदि मूलतः एलिअन ही हैं, वह स्वर्ग से आते हैं और स्वर्ग को ही लौटते हैं या सारे ब्रह्माण्ड में इच्छानुसार पलक-झपकते डोलते रहते हैं.
तो माजरा यह है कि तीन पर्वताकार रकाबीनुमा खगोलयान राजस्थान पर मँडरा कर अपने एक यात्री को थार में दिगंबर छोड़ जाते हैं. नंगा-पुंगा सिर्फ़ इसलिए नहीं कि उसके गोले के निवासी ऐसे ही रहते हैं, बल्कि यूँ भी कि स्वानंद किरकिरे को एक और घटिया ‘लिरिक’ लिखने का मौक़ा मिल सके. सिर्फ़ उसकी गर्दन में एक स्फटिक का कोई स्वदेश-संपर्क-यंत्र है जो ऐसे एलिअन-नेटिव टूरिस्टों को चूतिया बनानेवाले जयपुर-जैसलमेर-बाड़मेर के किसी रँग-रँगीले शरारती एम्पोरियम से खरीदा हुआ लगता है. एक बदमाश राजस्थानी गाँववाला उसे ही झपट कर भाग जाता है. अब हमारा पीके एलिअन ‘फ़ोन होम’ नहीं कर सकता लेकिन उस के पास खोने के लिए सिर्फ़ ऑडियो-कैसेट वाला एक प्राचीन टू-इन-वन है. एक ईमानदार, जीवनदानी राजस्थानी बैंडबाजेवाला वचन देता है कि वह उसे उसका तावीज़ लौटवा कर ही दम लेगा.
राजकुमार हिरानी और आमिर ख़ान की फ़िल्म इसके बाद अपना मक़सद हासिल करती दिखाई गई है. पीके एलियन के गृहग्रह पर हिंदुस्तान जैसे हालात नहीं हैं. वहाँ भाषा नहीं है, लोग टेलीपैथी से बात करते हैं, वहाँ धर्म-कर्म नहीं हैं, ईश्वर या तो बहुत कम है या है ही नहीं, किसी किस्म की मूर्तियाँ और इबादतगाहें नहीं हैं, बाबा-साधू नहीं हैं, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ऊँच-नीच आदि का नामोनिशान नहीं है और स्त्री-पुरुषों को परस्पर प्रेम और विवाह करने की पूरी आज़ादी है, परिवार और समाज उसके आड़े नहीं आते. जब पीके एलियन भारत में यह सब होते देखता है तो तत्काल अपना अजेंडा तय कर लेता है.
सबसे पहले तो उसे यहाँ की कोई भाषा सीखनी है. इसका एक ही तरीक़ा है कि वह किसी सुन्दर औरत के दोनों हाथ पकड़े और छः घंटे तक दोनों ऐसे ही चुप बैठे या लेटे रहें ताकि उस महिला की पूरी भाषा किसी परामनोवैज्ञानिक, स्थायी पाणिनीय अष्टाध्यायी स्थानान्तरण के माध्यम से उसके मस्तिष्क में अंकित हो जाए. सच्चरित्र हिन्दू नारियाँ तो किसी पराये मर्द को अपना हाथ तक छूने नहीं देतीं, लिहाज़ा एक चकले में जाकर इसे अंजाम दिया जाता है, और आश्चर्य! वह उदारचरिता भोजपुरी मातृभाषा वाली है, तो हमारा चरितनायक उसी में निष्णात हो उठता है और जब तक भारतीय धरती पर रहता है, सबसे वही बोलता है. यह बात अलग है कि हिरानी-आमिर-पीके की भोजपुरी बहुतै गड़बड़ बा.
उपरोक्त अजेंडे में भारतीय समाज-सुधार तो शामिल करना ही है, साथ में उत्तरी यूरोप के ब्रूष शहर में पढ़ने वाली एक भारतीय हिन्दू युवती का मिलन और विवाह उसके उतने ही युवक किन्तु वहीं रहने और पाकिस्तानी एम्बेसी में काम करनेवाले मुस्लिम नौजवान प्रेमी से करवाना भी है. इसके लिए सारे धर्मों के पाखण्ड और अन्याय को बेनक़ाब करना होगा और सबसे ज़्यादा उन हिन्दुत्ववादी बाबाओं को, जो ऐसे प्रेम और विवाह को महापाप मानते हैं और हिन्दू परिवारों और समाज को वर्गलाते-भड़काते हैं. कहानी बताना हमारा उद्देश्य नहीं. उसके लिए फिल्म देखनी होगी जो उस लायक है.
फिल्म में ऐसी कई स्थितियाँ और संवाद हैं जिनसे किशोर और युवा दर्शक बहुत खुश होते हैं और तालियाँ-सीटियाँ बजाते हैं. यह आमिर खान के फर्स्ट-डे-फर्स्ट-शो वाले फैन हैं या पूरी फिल्म से प्रसन्न दर्शक जो इसे रिपीट करेंगे या वर्ड-ऑफ़-माउथ से इसका व्यापक प्रचार करेंगे यह कहना मुश्किल है. इसमें हिंसा, वल्गेरिटी, सस्तापन, नंगई, अर्ध-अश्लीलता आदि सलमानी-रजनीकान्तीय-प्रभुदैवीय तत्व नहीं हैं. एक लिहाज़ से यह फिल्म पारिवारिक और हर उम्र के ‘बच्चों’ के लिए भी है.
लेकिन यह कारुणिक और दयनीय है कि हमारे फिल्म-समीक्षक और दर्शक बेहूदा हिंदी फिल्मों से इतने आजिज़ आ चुके हैं, जबकि उन्हें देखते भी हैं और ‘हिट’ भी करवाते हैं, कि इसे एक महान या कालजयी फिल्म मानने-मनवाने पर आमादा हैं. जहालत इतनी है कि कहा जा रहा है कि राज कपूर, बिमल रॉय और गुरुदत्त इसे बनाकर गर्व महसूस करते. जबकि पीके ठीक उन्हीं मसलों से भागती है जिनसे सीधी मुठभेड़ ऐसे निदेशकों ने की थी. यह श्याम बेनेगल, गोविन्द निहलाणी, एम.एस. सत्यु, मुज़फ्फर अली, प्रकाश झा, तिग्मांशु धूलिया, विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप आदि का भी सिनेमा नहीं है.
आप देखें कि एलियन को इसलिए नायक बनाया गया है कि उसके राष्ट्र, कौम, नाम, धर्म, जात-उपजाति-खाप आदि की ज़रूरत ही न पड़े. वह जो उपदेश देता है या हरकतें करता है वह इस सन्दर्भहीनता में स्वीकार्य हो जाती हैं. जादूगरी की भाषा में इसे ‘स्लाइट-ऑफ़-हैण्ड’ – हाथ की सफ़ाई – कहते हैं. यह सही है कि कुछ दुस्साहसपूर्ण बातें कही गई हैं लेकिन वह एक आसाराम-रामदेव-राजपाल आदि जैसे एक ‘तपस्वीजी’ बाबा को लेकर हैं और वैसी बातों से खुद उनके असली अनुयायियों को लेकर कोई आपत्ति नहीं होती, जो मानते हैं कि ‘हमारे अवतारी बाबा ऐसा नहीं करते’.
राजनीति, हिंसा और आतंकवाद आदि को लेकर इस फिल्म में एक भयावह डरी हुई चुप्पी है. देश में इतना बड़ा राजनीतिक बदलाव आया जिस पर पीके कुछ नहीं कहती. भारत-पाकिस्तान के हिन्दू-मुसलमानों के बीच रोटी-बेटी का रिश्ता न हो पाना क्या सियासत का एक नतीजा नहीं? और क्या हिन्दुस्तान में ही ऐसी मुहब्बतें और निकाह गली-गली हो रहे हैं? क्या हिन्दू-ईसाई-सिख-जैन-बौद्ध शादियाँ आसान हैं? अभी कल ही जो हाइकोर्ट का शादी बरक्स धर्म-परिवर्तन वाला लव-जिहादी फ़ैसला आया है, उसका क्या? एक अजीब बम-विस्फोट दिखाकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आतंकवाद के सवाल पर एलियन चुप क्यों है?
यह फिल्म हिन्दुस्तान की ग़रीबी, भुखमरी और गलाज़त के मामलों पर गूँगी है. बलात्कार और भ्रूण-हत्याएँ भारतमाता के देश में होते ही नहीं. इस देश का एक भी नेता, अफ़सर और पुलिसवाला इसका बड़ा किरदार नहीं. यहाँ मीडिया के नाम पर एक टीवी चैनल है, अखबार हैं ही नहीं. मॉल और मल्टीनेशनल्स और कैपिटलिज्म का नामोनिशान नहीं. माफ़िया और बिल्डर इसमें नहीं होते. भ्रष्टाचार की हमने सफाई कर दी. स्विस खतों का भंडाफोड़ कभी का हो चुका. एक टुच्चे बाबा का भंडाफोड़ कर दीजिये, एक टेलीफोन बेल्जियम की पाकिस्तानी एम्बेसी से मिलाइए, वह आपको पिंडी से कनेक्ट कर देंगे, कुछ गिले-शिकवे-आँसू करवा दीजिए और सरफ़राज़ और उस जग्गो की शहनाइयाँ बजवा दीजिए जो पीके एलियन के लिए भी तड़पना शुरू कर चुकी है.
चूंकि मूलतः यह एक असंभव, फील-गुड, मॉडर्न परी-और-फ़ंतासी कथा है इसलिए हम इस तरह के सवाल ही नहीं उठा रहे हैं कि जो सभ्यता इतनी एडवांस्ड और संपन्न है कि तीन खगोलयान धरती के एटमोंस्फियर में भेज कर अपने एक ‘आदमी’ को यहाँ उतार सकती है उसने अपने ‘गोले’ में बैठ कर बरसों पहले सारी रेकी क्यों नहीं की. उनके यहाँ ‘औरतें’ होती हैं या नहीं? अपनी एक मादा को लेकर पीके यहाँ क्यों नहीं आया? क्या उसे भारत की बलात्कार हॉबी का पता था?
हिरानी और आमिर कहेंगे – फिल्म देखते हो या भाड़ झोंकते हो? आख़िरी शॉट में हमने नंगे पीके के साथ नंगा रणबीर और पांच-छः और नंगे एक्स्ट्रा भेजे हैं. यह पीके पार्ट वन है. रणबीर पार्ट टू होगा. एक्स्ट्रा अलग. पीके एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइज़ बनने जा रहा है. पार्ट सिक्स के बाद यह सारे अच्छे एलियन धरती के गोले की सारी प्रॉब्लमें सॉल्व कर देंगे –इंसानियत समेत. अभी तो तपस्वीजी वाला. इंडो-पाक वाला वगैरह कई मसले बचे हुए हैं. देखना, अभी तो जग्गू सरफ़राज़ को छोड़ेगी और पीके के साथ उड़ जाएगी. तुम बस खुद टिकट लेते रहो और दर्शकों से लिवाते रहो. द गुड एलियंस आर लैंडिंग.
(यह टिप्पणी नवभारत टाइम्स में कुछ परिवर्तनों के साथ प्रकाशित है. तस्वीर के लिए डीएनए का आभार. बुद्धू-बक्सा विष्णु खरे और अन्य सभी का आभारी.)
विष्णु खरे
मानव शुरू से ही अपने अस्तित्व की समस्याओं से इतना आक्रान्त रहा है कि उसे हर जगह और हर शय में अपने ईश्वर, बुत, फ़रिश्ते, उद्धारक, अवतार स्त्री-पुरुष और नबी-मसीहा खोजने पड़े हैं. विडंबना यह है कि समस्याएँ उतनी ही बढ़ती गई हैं जितने भगवान और पैग़म्बर आए हैं. बल्कि शायद यदि वे कम आए होते, या आते ही नहीं, तो इंसानियत की ऐसी दुर्दशा न होती. अभी जो डेढ़ सौ बच्चे मारे गए हैं उनके पीछे मजहबी थे. मेरठ-गुजरात में भी चोटी-जनेऊ-तिलक-कलावे वाले धर्मप्राण लोग ही बसते हैं. नाइजीरिया में इस्लामी ‘बोको हराम’ ने मानवता का जीना हराम कर रखा है.
जबसे ब्रह्माण्ड के आयामों का पता चला है तबसे यह उम्मीद भी बाँधी गई है कि शायद कहीं ऐसी नस्लें हों जो हम जैसी हों, हम से हजारों गुना विकसित हों, जो हमसे रूबरू या इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से संपर्क साधें और हमारे वुजूद की हिफ़ाज़त करें. हाय रे शिकस्ता ज़ेहनी गुलामी की मजबूरियाँ! लेकिन उसमें यह ख़तरा भी है कि कोई तालिबान, आइ.एस. या हिंदुत्वी-नुमा घुमंतू कायनाती आतंकवादी दस्यु बेड़ा भी हो, जो टेक्नोलॉजी में हमसे सदियों आगे हो लेकिन हर तरह के दूसरे प्राणियों को वाक़ई खाकर ही जिंदा रहता हो, तब हम क्या करेंगे?
जब ‘गाँधीगीरी’ फिल्मों में सुपरहिट रही और भारतीय यथार्थ में सुपरफ्लॉप, तो अब बारी आई है दूसरे ‘गोले’ से आए ‘नेकेड फ़कीर’ ‘पीके’ की. यह भी इसलिए आ सकी कि हमारी दोग़ली इंडस्ट्री के असली गोरे हॉलीवुडी अब्बामियाँ बरसों से विज्ञान-कथा (साइंस-फ़िक्शन) और अच्छे-बुरे एलिअनों का मुफ़ीद इस्तेमाल कर रहे हैं. यह बात अलग है कि अपने भोलेपन में पहली ग़लती सत्यजित राय ने की और हमने अपना ‘महाभारत’ सही ढंग से अब तक नहीं पढ़ा. वैसे हिन्दू मिथकों में सारे भगवान, देवी-देवता, अवतार, ऋषि-मुनि आदि मूलतः एलिअन ही हैं, वह स्वर्ग से आते हैं और स्वर्ग को ही लौटते हैं या सारे ब्रह्माण्ड में इच्छानुसार पलक-झपकते डोलते रहते हैं.
तो माजरा यह है कि तीन पर्वताकार रकाबीनुमा खगोलयान राजस्थान पर मँडरा कर अपने एक यात्री को थार में दिगंबर छोड़ जाते हैं. नंगा-पुंगा सिर्फ़ इसलिए नहीं कि उसके गोले के निवासी ऐसे ही रहते हैं, बल्कि यूँ भी कि स्वानंद किरकिरे को एक और घटिया ‘लिरिक’ लिखने का मौक़ा मिल सके. सिर्फ़ उसकी गर्दन में एक स्फटिक का कोई स्वदेश-संपर्क-यंत्र है जो ऐसे एलिअन-नेटिव टूरिस्टों को चूतिया बनानेवाले जयपुर-जैसलमेर-बाड़मेर के किसी रँग-रँगीले शरारती एम्पोरियम से खरीदा हुआ लगता है. एक बदमाश राजस्थानी गाँववाला उसे ही झपट कर भाग जाता है. अब हमारा पीके एलिअन ‘फ़ोन होम’ नहीं कर सकता लेकिन उस के पास खोने के लिए सिर्फ़ ऑडियो-कैसेट वाला एक प्राचीन टू-इन-वन है. एक ईमानदार, जीवनदानी राजस्थानी बैंडबाजेवाला वचन देता है कि वह उसे उसका तावीज़ लौटवा कर ही दम लेगा.
राजकुमार हिरानी और आमिर ख़ान की फ़िल्म इसके बाद अपना मक़सद हासिल करती दिखाई गई है. पीके एलियन के गृहग्रह पर हिंदुस्तान जैसे हालात नहीं हैं. वहाँ भाषा नहीं है, लोग टेलीपैथी से बात करते हैं, वहाँ धर्म-कर्म नहीं हैं, ईश्वर या तो बहुत कम है या है ही नहीं, किसी किस्म की मूर्तियाँ और इबादतगाहें नहीं हैं, बाबा-साधू नहीं हैं, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ऊँच-नीच आदि का नामोनिशान नहीं है और स्त्री-पुरुषों को परस्पर प्रेम और विवाह करने की पूरी आज़ादी है, परिवार और समाज उसके आड़े नहीं आते. जब पीके एलियन भारत में यह सब होते देखता है तो तत्काल अपना अजेंडा तय कर लेता है.
सबसे पहले तो उसे यहाँ की कोई भाषा सीखनी है. इसका एक ही तरीक़ा है कि वह किसी सुन्दर औरत के दोनों हाथ पकड़े और छः घंटे तक दोनों ऐसे ही चुप बैठे या लेटे रहें ताकि उस महिला की पूरी भाषा किसी परामनोवैज्ञानिक, स्थायी पाणिनीय अष्टाध्यायी स्थानान्तरण के माध्यम से उसके मस्तिष्क में अंकित हो जाए. सच्चरित्र हिन्दू नारियाँ तो किसी पराये मर्द को अपना हाथ तक छूने नहीं देतीं, लिहाज़ा एक चकले में जाकर इसे अंजाम दिया जाता है, और आश्चर्य! वह उदारचरिता भोजपुरी मातृभाषा वाली है, तो हमारा चरितनायक उसी में निष्णात हो उठता है और जब तक भारतीय धरती पर रहता है, सबसे वही बोलता है. यह बात अलग है कि हिरानी-आमिर-पीके की भोजपुरी बहुतै गड़बड़ बा.
उपरोक्त अजेंडे में भारतीय समाज-सुधार तो शामिल करना ही है, साथ में उत्तरी यूरोप के ब्रूष शहर में पढ़ने वाली एक भारतीय हिन्दू युवती का मिलन और विवाह उसके उतने ही युवक किन्तु वहीं रहने और पाकिस्तानी एम्बेसी में काम करनेवाले मुस्लिम नौजवान प्रेमी से करवाना भी है. इसके लिए सारे धर्मों के पाखण्ड और अन्याय को बेनक़ाब करना होगा और सबसे ज़्यादा उन हिन्दुत्ववादी बाबाओं को, जो ऐसे प्रेम और विवाह को महापाप मानते हैं और हिन्दू परिवारों और समाज को वर्गलाते-भड़काते हैं. कहानी बताना हमारा उद्देश्य नहीं. उसके लिए फिल्म देखनी होगी जो उस लायक है.
फिल्म में ऐसी कई स्थितियाँ और संवाद हैं जिनसे किशोर और युवा दर्शक बहुत खुश होते हैं और तालियाँ-सीटियाँ बजाते हैं. यह आमिर खान के फर्स्ट-डे-फर्स्ट-शो वाले फैन हैं या पूरी फिल्म से प्रसन्न दर्शक जो इसे रिपीट करेंगे या वर्ड-ऑफ़-माउथ से इसका व्यापक प्रचार करेंगे यह कहना मुश्किल है. इसमें हिंसा, वल्गेरिटी, सस्तापन, नंगई, अर्ध-अश्लीलता आदि सलमानी-रजनीकान्तीय-प्रभुदैवीय तत्व नहीं हैं. एक लिहाज़ से यह फिल्म पारिवारिक और हर उम्र के ‘बच्चों’ के लिए भी है.
लेकिन यह कारुणिक और दयनीय है कि हमारे फिल्म-समीक्षक और दर्शक बेहूदा हिंदी फिल्मों से इतने आजिज़ आ चुके हैं, जबकि उन्हें देखते भी हैं और ‘हिट’ भी करवाते हैं, कि इसे एक महान या कालजयी फिल्म मानने-मनवाने पर आमादा हैं. जहालत इतनी है कि कहा जा रहा है कि राज कपूर, बिमल रॉय और गुरुदत्त इसे बनाकर गर्व महसूस करते. जबकि पीके ठीक उन्हीं मसलों से भागती है जिनसे सीधी मुठभेड़ ऐसे निदेशकों ने की थी. यह श्याम बेनेगल, गोविन्द निहलाणी, एम.एस. सत्यु, मुज़फ्फर अली, प्रकाश झा, तिग्मांशु धूलिया, विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप आदि का भी सिनेमा नहीं है.
आप देखें कि एलियन को इसलिए नायक बनाया गया है कि उसके राष्ट्र, कौम, नाम, धर्म, जात-उपजाति-खाप आदि की ज़रूरत ही न पड़े. वह जो उपदेश देता है या हरकतें करता है वह इस सन्दर्भहीनता में स्वीकार्य हो जाती हैं. जादूगरी की भाषा में इसे ‘स्लाइट-ऑफ़-हैण्ड’ – हाथ की सफ़ाई – कहते हैं. यह सही है कि कुछ दुस्साहसपूर्ण बातें कही गई हैं लेकिन वह एक आसाराम-रामदेव-राजपाल आदि जैसे एक ‘तपस्वीजी’ बाबा को लेकर हैं और वैसी बातों से खुद उनके असली अनुयायियों को लेकर कोई आपत्ति नहीं होती, जो मानते हैं कि ‘हमारे अवतारी बाबा ऐसा नहीं करते’.
राजनीति, हिंसा और आतंकवाद आदि को लेकर इस फिल्म में एक भयावह डरी हुई चुप्पी है. देश में इतना बड़ा राजनीतिक बदलाव आया जिस पर पीके कुछ नहीं कहती. भारत-पाकिस्तान के हिन्दू-मुसलमानों के बीच रोटी-बेटी का रिश्ता न हो पाना क्या सियासत का एक नतीजा नहीं? और क्या हिन्दुस्तान में ही ऐसी मुहब्बतें और निकाह गली-गली हो रहे हैं? क्या हिन्दू-ईसाई-सिख-जैन-बौद्ध शादियाँ आसान हैं? अभी कल ही जो हाइकोर्ट का शादी बरक्स धर्म-परिवर्तन वाला लव-जिहादी फ़ैसला आया है, उसका क्या? एक अजीब बम-विस्फोट दिखाकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आतंकवाद के सवाल पर एलियन चुप क्यों है?
यह फिल्म हिन्दुस्तान की ग़रीबी, भुखमरी और गलाज़त के मामलों पर गूँगी है. बलात्कार और भ्रूण-हत्याएँ भारतमाता के देश में होते ही नहीं. इस देश का एक भी नेता, अफ़सर और पुलिसवाला इसका बड़ा किरदार नहीं. यहाँ मीडिया के नाम पर एक टीवी चैनल है, अखबार हैं ही नहीं. मॉल और मल्टीनेशनल्स और कैपिटलिज्म का नामोनिशान नहीं. माफ़िया और बिल्डर इसमें नहीं होते. भ्रष्टाचार की हमने सफाई कर दी. स्विस खतों का भंडाफोड़ कभी का हो चुका. एक टुच्चे बाबा का भंडाफोड़ कर दीजिये, एक टेलीफोन बेल्जियम की पाकिस्तानी एम्बेसी से मिलाइए, वह आपको पिंडी से कनेक्ट कर देंगे, कुछ गिले-शिकवे-आँसू करवा दीजिए और सरफ़राज़ और उस जग्गो की शहनाइयाँ बजवा दीजिए जो पीके एलियन के लिए भी तड़पना शुरू कर चुकी है.
चूंकि मूलतः यह एक असंभव, फील-गुड, मॉडर्न परी-और-फ़ंतासी कथा है इसलिए हम इस तरह के सवाल ही नहीं उठा रहे हैं कि जो सभ्यता इतनी एडवांस्ड और संपन्न है कि तीन खगोलयान धरती के एटमोंस्फियर में भेज कर अपने एक ‘आदमी’ को यहाँ उतार सकती है उसने अपने ‘गोले’ में बैठ कर बरसों पहले सारी रेकी क्यों नहीं की. उनके यहाँ ‘औरतें’ होती हैं या नहीं? अपनी एक मादा को लेकर पीके यहाँ क्यों नहीं आया? क्या उसे भारत की बलात्कार हॉबी का पता था?
हिरानी और आमिर कहेंगे – फिल्म देखते हो या भाड़ झोंकते हो? आख़िरी शॉट में हमने नंगे पीके के साथ नंगा रणबीर और पांच-छः और नंगे एक्स्ट्रा भेजे हैं. यह पीके पार्ट वन है. रणबीर पार्ट टू होगा. एक्स्ट्रा अलग. पीके एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइज़ बनने जा रहा है. पार्ट सिक्स के बाद यह सारे अच्छे एलियन धरती के गोले की सारी प्रॉब्लमें सॉल्व कर देंगे –इंसानियत समेत. अभी तो तपस्वीजी वाला. इंडो-पाक वाला वगैरह कई मसले बचे हुए हैं. देखना, अभी तो जग्गू सरफ़राज़ को छोड़ेगी और पीके के साथ उड़ जाएगी. तुम बस खुद टिकट लेते रहो और दर्शकों से लिवाते रहो. द गुड एलियंस आर लैंडिंग.